सवारी साइकिल की थी, पर शान शहंशाहों की थी

देवेन्द्रराज सुथार, जालोर. 'मेरा भी कभी-कभी / मन डगमगाता है / लगता हूं सोचने / कि ले लूं मोटरसाइकिल / आफिस में इज्जत बढ़ जायेगी / मानेंगे गरीब नहीं / लोग आसपास के / घण्टों का समय और / शक्ति भी बच जायेगी / लगती आने-जाने में जो / तीस किलोमीटर दूर। / लेकिन फिर लगता है / बिगड़ता ही जाता है / दिन-दिन जो पर्यावरण / मैं भी हुआ शामिल यदि / बढ़ाने में प्रदूषण तो / अपनी ही नजरों में / कैसे उठ पाऊंगा / कविता फिर कैसे लिख पाऊंगा?'
कवि हेमधर शर्मा की ये पंक्तियां एक ऐसे अंतर्द्वंद्व की झलक देती हैं, जो आज हर संवेदनशील इंसान के दिल में मचलता है। कभी वह दौर था जब मोहल्ले में किसी के पास साइकिल होना एक मुकम्मल हैसियत की पहचान था। स्कूल मास्टर हों या दफ्तर जाने वाले बाबू, सबका सपना होता था अपनी साइकिल होना। वह सिर्फ़ एक सवारी नहीं थी, बल्कि एक रवायत, एक तहज़ीब, एक सादगी का प्रतीक थी। साइकिल पर सवार होते हुए आदमी यूं मालूम होता जैसे वह बादशाह हो, जिसके पास वक़्त भी है, खुद्दारी भी और फ़िज़ाओं से मुहब्बत करने का सलीक़ा भी।
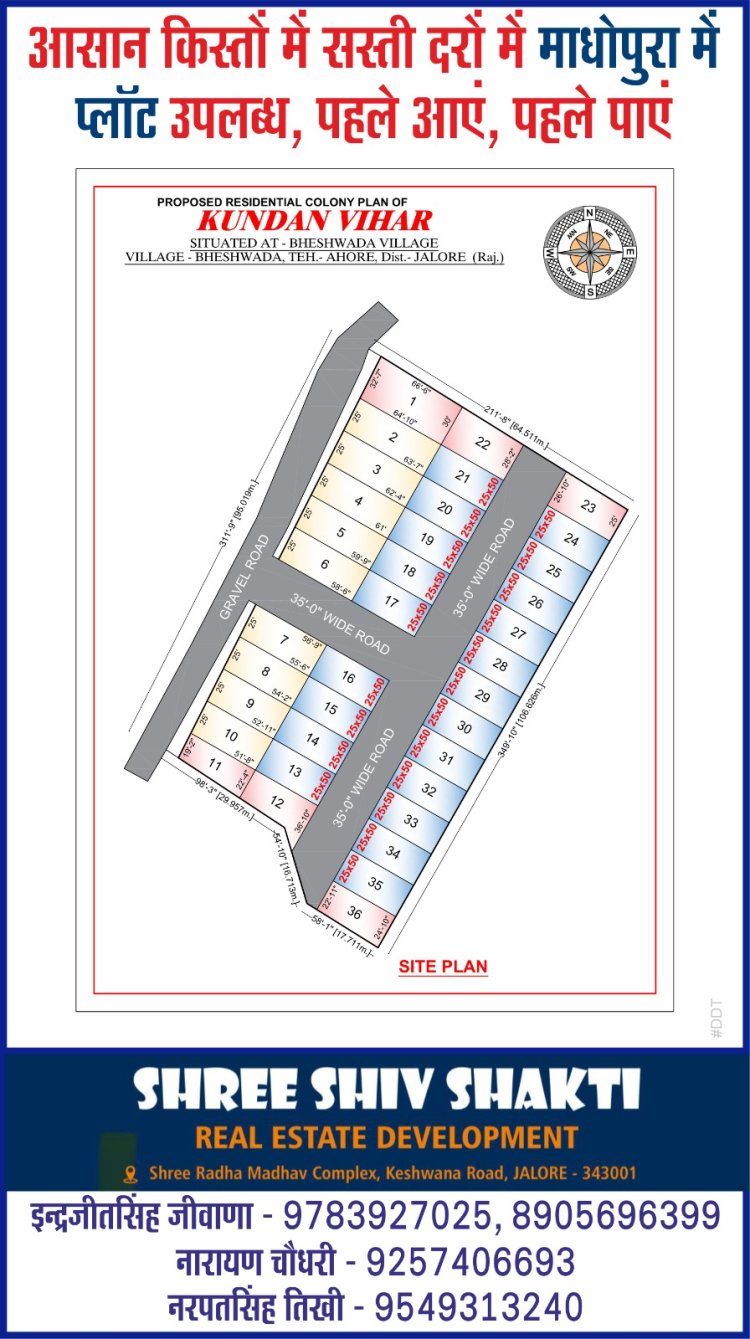
विज्ञापन
लेकिन वक़्त के साथ साइकिल का वह जादू मानो गर्द में दब गया। मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर ये तमाम तेज़ रफ़्तार और चमकदार ज़रिए अब हमारी ज़रूरत नहीं, हमारी पहचान बन गए हैं और पहचान की इस होड़ में हम ये भूलते जा रहे हैं कि इस रफ़्तार के पीछे हम क्या-क्या खो रहे हैं- ताजगी, सुकून, सेहत और सबसे बढ़कर हमारी धरती की सांसें।
आज जब जलवायु परिवर्तन वैश्विक संकट का रूप ले चुका है, जब शहरों की हवाओं में जहर घुल चुका है, ऐसे में साइकिल फिर से उम्मीद की एक किरण बनकर उभर रही है। यह वह साधन है जो ना ईंधन मांगता है, ना धुआं छोड़ता है और ना ही रास्तों को जाम करता है। साइकिल चलाना महज़ एक पर्यावरणीय निर्णय नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है- अपनी ज़मीन, अपने आकाश और अपनी अगली नस्लों के लिए।
हमें साइकिल को फिर से उसका वही पुराना मुक़ाम लौटाना होगा- जब वह सादगी में भी रईसी का आलम रखती थी, जब उस पर सवार होकर आदमी खुद को भी और दुनिया को भी बेहतरी की ओर ले जाता था। यह केवल संसाधन नहीं, एक अंदाज़-ए-ज़िंदगी है। आज जब जीवन तेज़ रफ्तार में बिखर रहा है, तब साइकिल एक ऐसा साज़ है जो हमारी रूह को सुरों में पिरो सकता है।

विज्ञापन
तो आइए, हेमधर शर्मा की तरह हम भी अपने भीतर झांकें। सोचें कि क्या सचमुच एक मोटरसाइकिल हमारे आत्मसम्मान की गारंटी है या फिर वह पसीने की महक, जो साइकिल चलाते हुए आती है- कहीं ज़्यादा पाक़ीज़ा नहीं? क्या वह पैडल मारते हुए गुज़रते रास्तों की हवा, पेड़ों की सरसराहट और अपने ही दिल की आवाज़ हमें कोई और सवारी दे सकती है? हमें इस सवाल का जवाब खुद से देना होगा और वह भी ईमानदारी से। क्योंकि अगर हम खुद की नजरों में गिर गए, तो फिर कविता कैसे लिख पाएंगे?










